Modern vs traditional child stories in hindi
(उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका 'साहित्य भारती' के अप्रैल-जून, 2012 अंक में प्रकाशित लेख)
सिर्फ हिन्दी ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं में बाल कहानी के विकास में ‘पंचतंत्र‘ का योगदान रहा है। ‘पंचतंत्र‘ में पशु-पक्षियों को आधार बनाकर कहानियों का सृजन किया गया था। जैसे-जैसे इन कथाओं का प्रसार होता गया, लोगों को कहानियों की शक्ति और आवश्यकता का एहसास हुआ। फलस्वरूप लोगों ने अपने उर्वर मस्तिष्क के द्वारा कहानियों को गढ़ना शुरू कर दिया। मानव की इन कल्पनाओं में पशु-पक्षियों ने जहाँ स्वाभाविक रूप से स्थान प्राप्त किया, वहीं समकालीन राज परिवार और उनके आकर्षणों ने भी जगह बनाने में सफलता हासिल की। फिर बाद में धीरे-धीरे मनुश्य की आकाँक्षाओं और अभिलाषाओं ने पैर पसारे तो कहानियों में जादू-टोना, राक्षस-जिन्न और परियों का भी समावेश होता चला गया।
जन अभिरूचि के फलस्वरूप जन्मी ये कहानियाँ कालांतर में ‘लोक कथाएँ’ और ‘परी कथाएँ’ के नाम से जानी गयीं। ये कहानियाँ मौखिक रूप से एक से दूसरे और तीसरे व्यक्ति के द्वारा हजारों वर्षों की यात्रा करती रही हैं। इनमें मौजूद कल्पना तत्व जहाँ पाठकों को बाँधता रहा है, मानवीय इच्छाओं का प्रस्फुटन इन्हें जीवनी शक्ति प्रदान करता रहा है। हजारों साल पुरानी इन कथाओं के अभी तक बचे रहने का यही प्रमुख कारण है।
किन्तु परिवर्तन के रथ पर सवार समाज में जब विज्ञान की बेशुमार प्रगति के कारण नये वातावरण का सृजन हुआ, तो नए सामाजिक, आर्थिक और साँस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप पुरानी मान्यताएँ और रूढ़ियाँ ढ़हने लगीं। परिवर्तन के इस युग में जहाँ कुछ लोगों ने पुराने मूल्यों से चिपके रहना उचित समझा, वही कुछ लोगों ने आगे बढ़कर नए मूल्यों का स्वागत किया। इन बदलते हुए हालात में जब जीवन जीने के तरीके बदल गये, जीवन की आवश्यकताएँ बदल गयीं, जीवन के प्रति सोच बदल गयी, तो फिर हजारों वर्षों से चली आ रही लोक कथाएँ/परी कथाएँ वही कैसे रह सकती थीं? उनकी उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक ही था। यही कारण था कि आधुनिकतावादी विद्वानों ने इनकी सार्थकता पर न सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाए, वरन इन्हें बच्चों के लिए त्याज्य ही घोषित कर दिया।
हिन्दी के चर्चित और प्रयोगवादी बाल कथाकार मनहर चौहान ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि ‘‘बालक को परी कथाओं से सदैव दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई विशेष लाभ नहीं है। आज सामयिक महत्व की कथाएँ बालक को सुनाई जाएँ, तो उसका लहू खौल उठेगा और साहस उत्पन्न होगा तथा उसकी बुद्धि तो विकसित होगी ही, साथ ही एक नया अनुभव होगा। आज के वैज्ञानिक युग में बालकों के बौद्धिक सरोकार एवं आत्मिक बल के विकास के लिए उन्हें परी कथाओं से दूर ही रखना श्रेष्ठा है।‘‘1
इस आवाहन के फलस्वरूप जहाँ कुछ रचनाकार परी कथाओं को त्यागकर आधुनिक मूल्यों पर आधारित रचनाक्रम की ओर उन्मुख हो गये, वहीं तमाम लेखकों ने संस्कृति के नाम पर ऐसी कथाओं का लेखन जारी रखा।
प्राचीन कथाओं की विश्वसनीयता पर बड़े ही नहीं बच्चे भी प्रश्न उठाते रहे हैं। कम्प्यूटर और रोबोट की दुनिया से बाखबर बच्चों के लिए परियों का जादू व्यर्थ की चीज है। उन्हें मालूम है कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई और विज्ञान के चमत्कारों के बल पर ही दिखाया जा सकता है। इसीलिए परियों के चमत्कार उसे बिलकुल प्रभावित नहीं करते।
आज के बच्चे वास्तव में ज्यादा अक्लमंद और मेधा सम्पन्न हैं। वे सिर्फ कहानी सुनते या पढ़ते नहीं है, बल्कि अपनी तर्कशील दृष्टि से कहानी के परिवेश, पात्र और घटनाओं को परखता भी चलते हैं। उन्हें मालूम है कि इस सृष्टि में कहीं पर भी परीलोक नहीं हैं, उन्हें यह भी ज्ञात है कि जादू जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वे सिर्फ विज्ञान की शक्ति को जानते व मानते हैं। उन्हें अब वे कहानियाँ नहीं रास रातीं, जिनकी पात्र परियाँ होती हैं और जहाँ जादू की छड़ी से बड़े से बड़े काम चुटकी बजाते सम्पन्न हो जाते हैं। उन्हें वे ही कहानियाँ विश्वतसनीय लगती हैं, जिनके पात्र अंतरिक्षयान के द्वारा एक ग्रह से दूसरे ग्रहों की सैर करते हैं और वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा अपने कार्य सम्पन्न करते हैं।
आज का बच्चे बड़ों की बताई बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते, वह उन्हें अपने तर्क की कसौटी पर कसते हैं। और ऐसा न होने पर वह सीधे-सीधे अपनी असहमति दर्ज कराते हैं। उसे थोपे गये थोथे आदर्श, हिटलरी आदेश और अंध-विश्वास से भरी बातें बिलकुल भी स्वीकार नहीं होतीं। वह अपने संदेहों का तार्किक ढ़ंग से निराकरण चाहते हैं।
जबकि प्राचीन कथाएँ आज भी सामंती मूल्यों की पोषक बनी हुई हैं। वे समतावदी समाज की विरोधी हैं। इसके हजारों उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस तरह की कितनी ही कहानियों को पढ़ डालिए, सब में राज परिवार महिमामण्डित होता हुआ मिलेगा और यदि कहीं अपवाद स्वरूप राजा ‘नालायक’ भी हुआ, तो किसी साधु, मुनि या देवता की ‘कृपा‘ से सुधर कर महान बन जाएगा। यानी कि राजा-राजा है। वह आम आदमी से श्रेष्ठ है। उसे आदर-सम्मान मिलना ही चाहिए, उसकी पूजा होनी ही चाहिए।
यहाँ सवाल यह उठता है कि आज के प्रजातांत्रिक युग में इस सब का औचित्य क्या है? सीधी सी बात है कि भले ही सामंती युग समाप्त हो गया हो, पर उसे चाहने वाले अब भी स्वयं को बौद्धिक स्तर पर उससे अलग नहीं कर पाए हैं और वे बच्चों को इस तरह की कहानियाँ परोस कर उनके कोमल मन पर यह बात अंकित करना चाहते हैं कि आज के दौर की तुलना में राजा-रानी का युग कहीं बेहतर था।
आज समानता का युग है, जिसमें स्त्रियाँ भी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में तो वे स्वयं को पुरूषों से भी बेहतर साबित कर रही हैं। इस सबके बावजूद परी कथाओं में आज भी सिर्फ नारी पात्रों को ‘सजते-संवरते‘ हुए दिखाया जाता है। इन कथाओं में आए अधिकांश स्त्री पात्र शो-पीस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उनका काम ही है सजना-संवरना और पति की सेवा करना। फिर वह चाहे व्यापारी की पुत्री हो, राजा की बेटी हो या कोई परी। और परियों की अवधारणा तो खासकर हुई ही इसलिए है। इन सबके पीछे इन सामंती रचनाकारों की मानसिकता का एक मात्र उद्देश्य है आज कल की लड़कियों को अन्य कामों से मोड़कर सजने-संवरने में लगाना ताकि वह पढ़-लिख कर आगे बढ़ने के बजाए शो-पीस बनकर पुरूष जाति की भोग्या बनी रहें। तभी तो इन स्त्री पात्रों की परिणति होती है सिर्फ विवाह के रूप में। इससे इतर या इससे श्रेष्ठ उद्देश्य कोई होता ही नहीं-
‘राजा बहुत खुश हुआ। उसने पुष्कर को आधे राज्य का मालिक बनाकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह भी कर दिया। पुत्र वियोग में पागल राजा शिवसेन तथा महारानी भानुप्रिया ने जब यह खबर सुनी, तो खुशी से नाच उठे। वे दल-बल के साथ सूर्यगढ़ आए। फिर शुभ घड़ी देखकर राजकुमार चित्रसेन की शादी राजकुमारी चित्राँगदा से कर दी।’2
सन 1947 में आजाद मिलने के बाद भले ही इस देश का हर छोटा-बड़ा, ऊँचा-नीचा नागरिक आजाद और कानूनी रूप से समान अधिकार रखता हो, पर न सिर्फ स्त्री जाति वरन समाज के निम्न वर्ग के लोगों के विरूद्ध भी ये परी कथाएँ लामबंद नजर आती हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कृष्ण कुमार इसी चिंता को रेखाँकित करते हुए कहते हैं-
‘पुराणों और इतिहास के चरित्र आख्यानों में राजनीतिक संस्कारों के सामंतीपन की दिक्कत के अलावा एक अन्य दिक्कत उनके यौन संस्कारों से पैदा होती है। नायकों का नायिकाओं के प्रति दृष्टिकोण तथा सावित्री जैसी पत्नियों का आदर्श प्राथमिक शाला के बच्चों में दुर्भाग्यपूर्ण विसंगतियाँ पैदा कर सकता है। भारत में नारी और पुरूष की असमान सामाजिक स्थिति सामंती अतीत से उपजी है। जब हम राजानीति में सामंतवाद के विरूद्ध हैं, तो सामाजिक संदर्भ में उसके पक्षधर नहीं हो सकते। दुष्यंत और शकुंतला, सावित्री-सत्यवान, नल-दमयंती और राम-सीता की कहानियाँ उस समाज की हैं, जिसमें प्रेम की शुरूआत, पत्नी का संरक्षण तथा उसकी परीक्षा लेने का अधिकारी सभी कुछ पुरूष के अधीन है।‘‘3
आज के प्रजातांत्रिक युग में भी परी कथाएँ/पुराण कथाएँ एक खास वर्ग के विशेषाधिकारों और उनकी ‘सनक‘ को सही ठहराने में व्यस्त दीखती हैं-
‘इन्द्र ने अपने विशिष्ट अतिथि के मनोरंजन के लिए नीलम परी को बुलवा भेजा। जिस समय देवेन्द्र का दूत नीलम परी के पास पहुँचा, उस समय वह दर्पण के सामने खड़ी अपने ही प्रतिबिम्ब को निहार रही थी। दूत तो संदेश देकर चला गया, लेकिन नीलम परी आत्म-मुग्ध की उसी अवस्था में खड़ी रही। ...यह देखकर इन्द्र बहुत क्रोध्रित हुए। ...वह बोले- ‘हम उसे श्राप देते हैं कि जिस सुंदरता पर उसे इतना घमण्ड है, वह इसी क्षण कुरूपता में बदल जाए।’4
इस प्रकार के प्रसंग क्या कहते हैं? जिसके पास शक्ति है, वह जिसके साथ जैसा चाहे बर्ताव कर सकता है? वह चाहे किसी को मिटा दे, चाहे किसी को नेस्तानाबूद कर दे? यही न? और ये सब इसलिए कि वह श्रेष्ठ है? ऊँचे पद पर बैठा है? क्या बच्चों को यही पढ़ाना चाहिए? और क्या वे इससे यह नहीं सीखेंगे कि यदि तुममें सामर्थ्य है, तो तुम हर उस व्यक्ति के साथ मनमानी करने के अधिकारी हो, जो तुमसे कमजोर हो?
परी कथाओं के नाम पर बच्चों को क्या-क्या परोसा जा रहा है, इसे देखकर पाठक सिहर उठता है।
‘सिर पर गदा’ इसी भाव से लिखी गयी एक खतरनाक कहानी है-
‘प्राचीन समय में वज्राँग नाम का एक महाबली दैत्य था। दैत्य होते हुए भी वह शान्तिप्रिय था। वज्रांग जब तपस्या में लीन था, तो देवराज इन्द्र ने (उसकी पत्नि) वाराँगी को अनेक यातनाएँ दीं। वज्राँग की समाधि जब टूटी, तो वाराँगी ने पति को इन्द्र की यातनाओं के बारे में बताया’
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वज्राँग ‘शान्ति प्रिय‘ दैत्य था। लकिन फिर भी इन्द्र ने उसकी पत्नी को यातनाएँ दीं और वह भी तब, जब वह तपस्या कर रहा था। और एक पुरूष एक स्त्री को किस प्रकार की ‘यातनाएँ’ दे सकता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्द्र ने ऐसा ही किया, क्योंकि वह देवताओं का राजा था, श्रेष्ठ था और उसे किसी के साथ भी मनमानी करने का अधिकार प्राप्त था?
ऐसी कहानियाँ आज के युग में क्या शिक्षा दे रही हैं?
बाद में अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए वाराँगी के पुत्र ने जब इन्द्र को पकड़ कर अपनी माँ के सामने ला खड़ा किया, तो वह बोली- ‘बेटा, प्रसिद्ध व्यक्ति का अपमान उसके वध से भी अधिक दुखद होता है। इसलिए इन्द्र का मुण्डन कर उसे छोड़ दिया जाए।’
कहाँ देवराज की ‘लुच्चई‘ और कहाँ दानव की विनम्रता?
इस पर इन्द्र ने अपने ‘अपमान’ का बदला लेने हेतु ब्रह्मा की शरण ली और फिर जगत नियंता ब्र उन्हें उसकी युक्ति बताते हैं। वाराँगी के पुत्र का कार्तिकेय द्वारा वध करके इन्द्र अपने ‘अपमान’ का बदला लेने में सफल होते हैं।
....ये है ऊँचे कुल या वर्ग का दम्भ, जिसकी रक्षा में ‘जगत नियंता’ शक्तियाँ एक हो गयीं। और वे फिर होती क्यों नहीं? भला वे कैसे बर्दाश्त करते कि इस असुर उनके ‘विशेषाधिकारों’ की राह में अडंगा लगाए? वह ठहरा तो असुर ही। हेय और नीच। और देवता जैसे ‘श्रेष्ठ‘ लोगों ने अगर उनकी स्त्री को ‘प्रताड़ित’ कर ही दिया, तो कौन सी आफत आ गयी? इससे तो उनकी ‘शान‘ ही बढ़ी? आखिर देवराज ने वाराँगी को इस लायक तो समझा कि...।
लोक कथाओं/परी कथाओं मे छिपे यही वे तत्व हैं, जिनकी वजह से इन कथाओं के विरोध का स्वर मुखर हुआ और प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक कहानियों का जन्म हुआ।
इसके साथ ही साथ लोक कथाओं में हिंसा के सूत्र भी गहराई तक जमे पाए जाते हैं। अक्सर लोक कथाओं के नायक राजा अपने विरोधियों की जीभ कटवा देते हैं, उनकी आँखें निकलवा लेते हैं। लोक कथाओं मे खलनायक तो हिंसा के पुजारी जैसे प्रतीत होते हैं।
अक्सर लोक कथा की डायनें खून पीती हुई नजर आती हैं। कही-कहीं लोक कथाओं में राक्षस द्वारा बच्चों को भून कर खाने का जिक्र मिलता है। कुछ एक लोक कथाओं में देवताओं के सामने बलि का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ अक्सर लोककथाओं में यह भी पढ़ने को मिलता है कि अमुक राक्षण की जान किसी तोते में अटकी हुई है। ऐसे में कहानी का नायक बड़ी निर्ममता से तोते को तड़पा-तड़पा कर मारता है। हालाँकि यह हिंसा एक तरह से हिंसा के प्रतीक राक्षक के नाश के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन प्रकारान्तर से इस तरह की कहानियाँ पढ़कर बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर पड़ता है और वे हिंसा के प्रति संवेदनशून्य होने लगते हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि लोक कथाएँ/परी कथाएँ बच्चों के दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। बाल साहित्य का मूल उद्देश्य है बच्चों को संवेदनशील बनाना, ताकि वह एक अच्छे इंसान के रूप में जिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए सचेत रहे। किन्तु यहाँ पर उल्टा बच्चों को परोक्ष रूप में हिंसा की ओर धकेला जा रहा है। इसलिए इस तरह की कथाओं को बच्चों को परोसना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता।
आज के बच्चों की अपनी सोच है, अपनी जरूरत है और अपनी चुनौतियाँ हैं। भागमभाग की इस दुनिया में आज माँ-बाप के पास इतना समय नहीं है कि वे बच्चों के साथ वक्त बिताएँ। ऐसे में बच्चों के लिए ऐसा साहित्य आवश्यक हो जाता है, जो उसे पिता का प्यार और माँ का दुलार दे सके। आधुनिक बाल कहानियाँ इसी सोच और इसी नजरिए से लिखी जा रही हैं। ये बच्चों की एक ऐसी दुनिया होती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वे होते हैं। इसीलिए आधुनिक बाल कहानियों में मनोविज्ञान का विशेष महत्व होता है।
आधुनिक बाल कहानी की शुरूआत
जहाँ तक पहली आधुनिक कहानी की बात है, इसके लिए माधवराव सप्रे रचित ‘एक टोकरी भर मिट्टी‘ का नाम सामने आता है। यह कहानी अप्रैल 1901 में ‘छत्तीसगढ़ मित्र‘ में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इसके बावजूद आधुनिक भाव-बोध वाली कहानियों की वास्तविक शुरूआत स्वतंत्र्योत्तर युग में हुई। हाँ, छिटपुट रूप में इक्का-दुक्का ऐसी रचनाएँ देखने को मिलती रही हैं। इनमें से कुछ रचनाएँ इस प्रकार से हैं-
1. सूबे साहब का नौकरः जे0पी0 काँत विशारद, बाल विनोद (अक्टूबर 1944), पृष्ठः 411
2. गंदा लड़काः महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, बालसखा (अप्रैल 1945), पृष्ठः 105
3. नाशपाती वालाः दीनबंधु पाठक, बालसखा (अप्रैल 1945), पृष्ठः 109
4. बाल मनोविकासः बलराम वनमाली (बालसखा, मई 1947), पृष्ठः 156
‘सूबे साहब का नौकर’ एक मूर्ख लड़के की कहानी है, जो खुशी की सूचना दुःखी होकर देता है और दुःख भरी सूचना के समय लड्डू बाँटने लगता है। ‘गंदा लड़का’ एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो बिना दातून-मंजन किए खाना खाता है। लेकिन जब उसके मुँह से आने वाली दुर्गन्ध के कारण उसके साथी उसके साथ खेलने से इनकार कर देते हैं, तो उसे अपनी गल्ती का एहसास होता है।
‘नाशपाती वाला’ में लेखक ने वैज्ञानिक जानकारी को आधार बनाया है।
‘बाल मनोविकास’ कहानी बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर लिखी गयी एक उत्कृष्ट रचना है। ‘इस कहानी में लेखक ने बताया है कि मातृहीन अजय को सौतेली माँ हर समय ‘बोदा’ कहती थी, तो वह अपने आप को मूर्ख समझने लगा। हर वक्त ‘बुरा-बुरा‘ कहने से बच्चे का मनोबल गिर गया और वह सचमुच वैसा ही बन गया। कहानी का यह अंश देखिए-
‘अजय सोचता था, रोता था। उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं। किसी चीज को उठाता तो घबराते-घबराते चीज गिर जाती थी। गिरने की आवाज सुनते ही माँ गरज उठती, ‘बड़ा कामचोर है। तोड़ दी चीज। सोचता होगा कि एक बार चीज पटक दूंगा तो फिर काम न करना पड़ेगा। खाता तो है सबसे ज्यादा, कहाँ जाता है सब? न मालूम किसलिए जीता है?’ अजय सोचने लगाता, सचमुच मैं किसलिए जीता हूँ, यदि मर जाऊँ, तो बला टल जाए।
‘‘संयोगवश मौसी के आगमन और उसके गाँव जाने पर अजय की स्थिति बदल जाती है। सबसे अच्छा व्यवहार और प्यार मिलने पर वह पढ़ाई और खेलकूद में आगे निकल जाता है। अब वह मौसी का लाड़ला है। सहपाठी उसका साथ चाहते हैं और अध्यापक उसे प्यार करते हैं। अजय सोचता है- मेरे गाँव के मास्टर मुझे बूद्धू कहते थे। यहाँ के मास्टर मुझे बुद्धिमान समझते हैं। कौन सी बात सच है?’5
इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक बाल कहानी प्राचीन बाल कहानी से सर्वथा भिन्न है। प्राचीन बाल कथाओं के मूल में जहाँ पुराणों के आख्यान, राजा-रानी के प्रसंग, भूत-प्रेत, टोने-टोटके, राक्षस-चुड़ैल, चमत्कार आदि हैं, वहीं आधुनिक बाल कथाओं के मूल में बाल मनोविज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टि, बदलते जीवन मूल्य, सामाजिक विद्रूपताएँ, पर्यावरणीय समस्याएँ प्रमुख रूप से स्थानी पाती हैं। यही कारण है कि आज के बच्चे इन कहानियों को ज्यादा पसंद करते हैं।
यद्यपि तमाम रचनाकारों में अभी भी प्राचीन कथाओं के प्रति मोह बना हुआ है, फिर भी असंख्य रचनाकार ऐसे हैं, जिन्होंने आधुनिक बाल कहानियों के भण्डार को भरने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे प्रमुख रचनाकारों में हरिकृष्ण् देवसरे, मनोहर वर्मा, विष्णु काँत पाण्डेय, शोभनाथ लाल, श्रीप्रसाद, राष्ट्राबंधु, उषा यादव, अनंत कुशवाहा, यादराम रसेन्द्र, कृष्णा नागर, शकुंतला वर्मा, शंकर सुल्तानपुरी, कल्पनाथ सिंह, साबिर हुसैन, चित्रेश, जाकिर अली ‘रजनीश’, नयन कुमार राठी, भगवती प्रसाद द्विवेदी, क्षमा शर्मा, भैरूलाल गर्ग, मो0 अरशद खान, रमाशंकर, रॉबिन षॉ पुश्प, रोहिताश्व अस्थाना, संजीव जायसवाल ‘संजय’, कमल चोपड़ा, विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी, राजीव सक्सेना, बिलास बिहारी, विमला रस्तोगी, रस्किन बॉण्ड, सुधीर सक्सेना ‘सुधि‘, संजीव सक्सेना, मो0 साजिद खान, दिनेश पाठक शशि, प्रभात गुप्त, खुशहाल जैदी, दिनेश चमोला आदि के नाम लिये जा सकते हैं।
संदर्भ
1. परीकथाओं की प्रासंगिकता का सवाल-राष्ट्रीय समाचार फीचर्स नेटवर्क, 26 सितम्बर 1995
2. जाकिर अली ‘रजनीश’, परी कथाओं के निहितार्थ-उत्तर प्रदेश (मार्च 1999), पृष्ठः 43
3. राज समाज और शिक्षा, पृष्ठः 92
4. गंगा और नीलम परी - तारा (मा0), जनवरी 1999
5. डा0 कामना सिंह, स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी बाल साहित्य, पृष्ठः 110-111
Keywods: children stories in hindi, Fairy Tales, Interesting Stories, Modern Short Stories, Science Fiction Short Stories, Scientific Stories





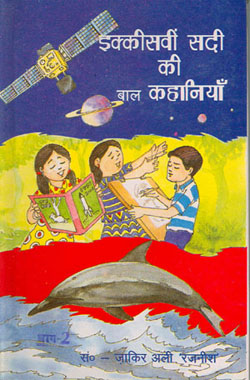










बढ़िया आलेख!
जवाब देंहटाएंsargarbhit prastuti...abhar
जवाब देंहटाएंबहुत बड़ा कलेवर है इस पोस्ट का पढने वाले के धैर्य की परीक्षा लेती है पोस्ट .बढिया तरीके से फर्क को समझाया गया है प्राचीन और आधुनिक बाल कथाओं के .मंतव्य को भी .अलबत्ता कहीं कहीं वर्तनी की अशुद्धियाँ रह गईं हैं छूट गईं हैं अनजाने ही .
जवाब देंहटाएंसृष्टि कर लें ब्रह्मांड के स्थान पर अशुद्ध रूप लिखा गया है .सृष्टि लिखना आसान है .'नामक' के स्थान पर नाम आयेगा .ब्रह्ममा आयेगा ब्रम्हा'के स्थान पर . ‘प्राचीन समय में वज्राँग 'नामक' का एक महाबली दैत्य था। दैत्य होते हुए भी वह शान्तिप्रिय था। वज्रांग जब तपस्या में लीन था, तो देवराज इन्द्र ने (उसकी पत्नि) वाराँगी को अनेक यातनाएँ दीं। वज्राँग की समाधि जब टूटी, तो वाराँगी ने पति को इन्द्र की यातनाओं के बारे में बताया’
इस पर इन्द्र ने अपने ‘अपमान’ का बदला लेने हेतु 'ब्रम्हा 'की शरण ली और फिर जगत नियंता 'ब्रम्हा' उन्हें उसकी युक्ति बताते हैं। वाराँगी के पुत्र का कार्तिकेय द्वारा वध करके इन्द्र अपने ‘अपमान’ का बदला लेने में सफल होते हैं।
बहर सूरत लेखक बधाई के सुपात्र है इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए .हम उनमे सदैव ही परफेक्शन देखतें हैं .
ज़र्रानवाज़ी का शुक्रिया। टाइपिंग मिस्टेक की ओर ध्यान दिलाने के लिए आभार। इससे पता चलता है कि पोस्ट ने वाकई आपके धैर्य की परीक्षा ली। :)
हटाएंबहुत सशक्त लेख |
जवाब देंहटाएंआशा
बढ़िया प्रस्तुति |
जवाब देंहटाएंबधाई ||
प्रभावशाली लेखन !
जवाब देंहटाएंस्तरीय आलेख है. लेखकीय श्रम साफ झलकता है. लेकिन लोककथाओं के प्रति अतिवादी द्रष्टिकोण भी लेख में है. लोकसाहित्य में केवल राजा—रानी, डायन और राक्षस की कहानियां ही नहीं हैं. उसमें भाई-भाई, भाई-बहन के प्रेम, ममता, वात्सल्य, लोक-न्याय और अन्याय को दर्शाती कहानियां भी हैं. किसी लोककथा में चींटी हाथी से टकराने का हौसला रखती है, तो एक और लोककथा में चिड़िया राजा को चुनौती दे डालती है. ये सब बैठे-ठाले का शगल या महज लेखकमन की कल्पना नहीं है. इनका प्रतीकात्मक महत्त्व भी है, जो समाज की जीवंतता को दर्शाता है. १८५७ के बाद देश ब्रिटिश सरकार के अधिपत्य में चला गया था. साढ़े पांच सौ से अधिक रजबाड़े अंग्रेजों के आगे समर्पण कर चुके थे. लेकिन इतिहास गवाह है कि 1857 से लेकर 1900 तक सौ से अधिक जनविद्रोह हुए थे, जिनका नेतृत्व समाज में मामूली कहे जाने वाले लोगों ने किया था. यह लोकसाहित्य की ताकत थी जो लोकस्मृति में समा, अवसर पाते ही अपना असर दिखाने लगती है. इसलिए लोकस्मृति से मुक्ति नहीं केवल उसमें परिष्करण की अवश्यकता है. बेहतर समाज की रचना के लिए वही श्रेयस्कर भी है. क्या बिना नींव के मजबूत इमारत बनाई जा सकती है?
जवाब देंहटाएंविज्ञान के जमाने में यह शायद संभव हो. हम आसानी से कह सकते हैं कि उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष में इमारत की कल्पना को सच किया जा सकता है. सवाल है कि क्या उसमें स्थायित्व होगा? फिर विज्ञान जो परोस रहा है, क्या वह सब का सब वरेण्य है. विज्ञान और तकनीक ने हमें बेहतर जीवन दिया है, इसमें संदेह नहीं. तकनीक सामंतवाद से मुक्ति का माध्यम भी बनी है, बन रही है—इसमें भी सचाई है. लेकिन इस तकनीक का विकृत रूप भी है. मैं विज्ञान का विरोधी नहीं. पर साहित्यकार के लिए विज्ञान की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टि अधिक उपयोगी है ऐसा मेरा मानना है. साहित्यकार को चाहिए कि वह वैज्ञानिक दृष्टि का समर्थन करे, न कि उसके द्वारा पैदा की गई सुविधाओं का. उस समय तक तो बिलकुल नहीं जब तक समाज में किसी भी प्रकार की असमानता है. वर्षों पहले सुनी एक कहानी याद आ रही है—
अमीर इब्राहीम एक बार अपने तख्त पर बैठा हुआ था. उसने छत पर हल्ला-गुल्ला और आवाजों का शोर सुना. अपने महल की छत पर उसे भारी-भरकम कदम भी सुनाई पड़े. वह सोचने लगा कि ये भारी-भरकम कदम किसके हैं? अपनी खिड़की से वह चिल्लाया—'
वहां कौन घूम-फिर रहा है?'
पहरेदारों ने सिर झुका लिए, बोले, 'हुजूर! हम कुछ ढूंढने के लिए चक्कर लगा रहे थे.'
'तुम क्या खोज रहे थे?' अमीर ने पूछा.
'अपने ऊंट!' पहरेदारों में से एक बोला.
'मूर्खो, क्या छत पर भी कोई ऊंट ढूंढता है?' अमीर गुस्साया. इसपर पहरेदारों ने गर्दन झुकाकर कहा—'हम आपका ही अनुसरण कर रहे हैं, जो तख्त पर बैठे-बैठे अल्लाह को पाना चाहते हैं.'
बहुत बाद में जान पाया कि कहानी फारसी के विद्वान जलालुद्दीन रूमी की है, अच्छे-अच्छों की आंख खोल देने वाले ऐसे अनमोल मोती लोककथाओं में भरे पड़े हैं.
इस टिप्पणी को एक ब्लॉग व्यवस्थापक द्वारा हटा दिया गया है.
जवाब देंहटाएंआदरणीय ओमप्रकाश जी, आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन लोककथाओं में जो अतिवाद गहरे से धंसा हुआ है, उसकी सफाई के लिए आलोचना के अतिवाद का ही सहारा लेना पडेगा, तभी शायद लोग उन चीजों की ओर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है।
जवाब देंहटाएं"बढिया से भी बढिया चर्चा ,प्रस्तुति .
जवाब देंहटाएंकृपया यहाँ भी पधारें -
शुक्रवार, 6 जुलाई 2012
वो जगहें जहां पैथोजंस (रोग पैदा करने वाले ज़रासिमों ,जीवाणु ,विषाणु ,का डेरा है )
विचारोत्तेजक प्रस्तुति के लिए बधाई एवं साधुवाद ।
जवाब देंहटाएंज़र्रानवाज़ी का शुक्रिया।
जवाब देंहटाएं